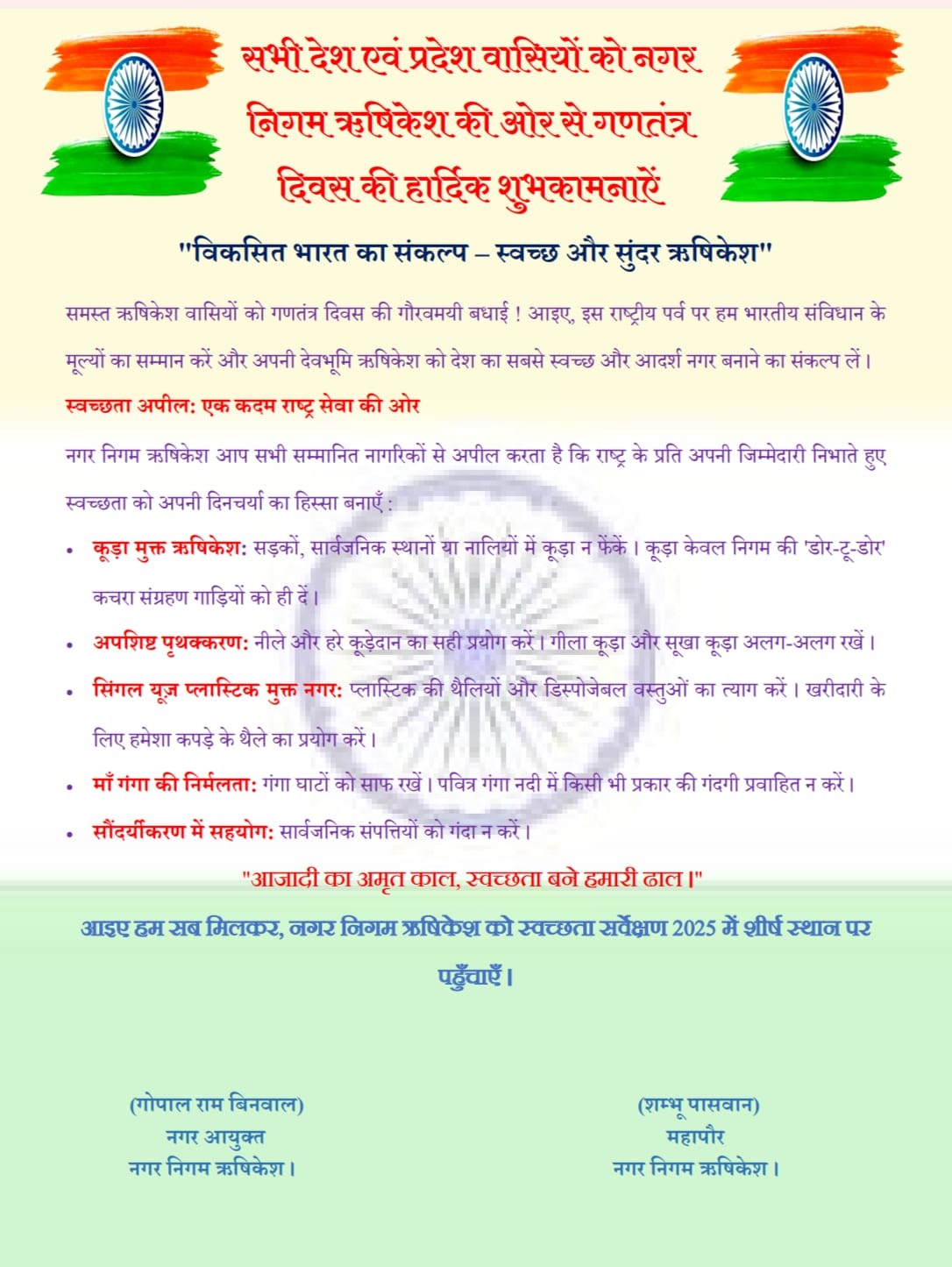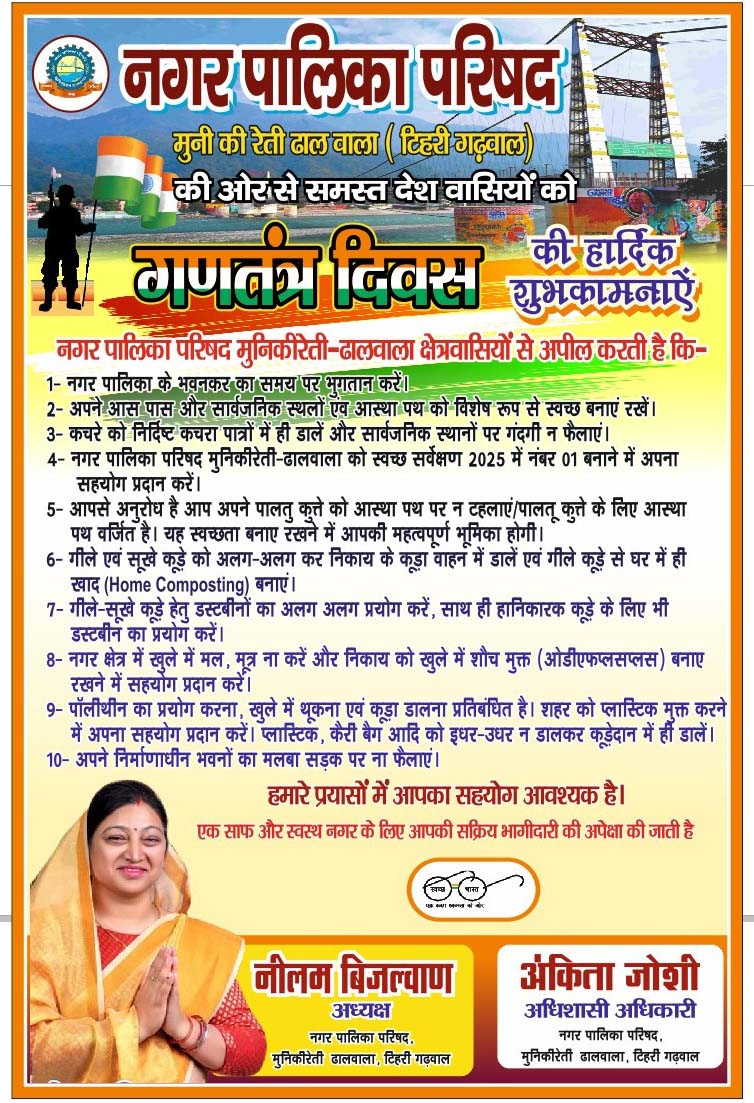Shrinagar: प्रसिद्ध बैकुंठ चतुर्दशी मेले का विधिवत आगाज
राज्यपाल ने वर्चुअल माध्यम से किया शुभारंभ, मंत्री डॉ. धन सिंह रावत रहे मौजूद

श्रीनगर गढ़वाल। प्रसिद्ध बैकुंठ चतुर्दशी मेला एवं विकास प्रदर्शनी 2023 का विधिवत आगाज हो गया। राज्यपाल लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह ने वर्चुअल माध्यम से मेले का शुभारंभ किया। कहा कि पहाड़ के पड़ाव पर इस मेले से संस्कृति और स्थानीय उत्पादों को देश दुनिया में पहचान मिलेगी।
शनिवार को चतुर्दशी के पर्व पर आवास विकास मैदान में बैकुंठ चतुर्दशी मेला एवं विकास प्रदर्शनी 2023 के शुभारंभ राज्यपाल लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह ने वर्चुअल माध्यम से अपने संबोधन में कहा कि श्रीनगर गढ़वाल क्षेत्र का मुख्य पड़ाव है, यहां पर इस प्रकार के मेलों के आयोजन के माध्यम से युवा पीढ़ी को सांस्कृतिक विरासत को समझने का अवसर मिलेगा। साथ हीं स्थानीय उत्पादों को देश-विदेश में पहचान मिलेगी। 
कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि श्रीनगर मंदिरों का सर्किट है, जिसमे 21 मंदिर शामिल है। यह श्रीनगर के धार्मिक रूप में उन्नति और उसके महत्व को दर्शाते हैं। इन मंदिर समूहों के संरक्षण व जीर्णोद्धार के लिए 16 करोड रुपये स्वीकृत किए गए हैं। कहा कि अगले वर्ष 02 करोड रुपये की लागत से कमलेश्वर महादेव मंदिर का सौन्दर्यकरण व जीर्णोद्धार कराया जाएगा।
उन्होंने उत्तर प्रदेश के नाम पर दर्ज आवास विकास मैदान को उत्तराखंड सरकार को हस्तांतरित करने के लिए डीएम को कार्यवाही करने को कहा। कहा कि आवास विकास मैदान सरकार को हस्तांतरित होने के बाद इसे नगर निगम श्रीनगर के अधीन किया जाएगा। कहा कि मेले को राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए आगे भी निरंतर भव्यता से मनाया जाएगा। मंत्री ने इससे पूर्व कमलेश्वर महादेव मंदिर में पूजा-अर्चना की। 
मौके पर जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान, डीआईजी एसएसबी सुभाष चंद नेगी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्वेता चौबे, मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य चंद्र मोहन नेगी, उपजिलाधिकारी नूपूर वर्मा, कमलेश्वर मंदिर के महंत आशुतोष पूरी, नागेश्वर महादेव मंदिर के महंत नितिन पूरी, जिलाध्यक्ष बीजेपी सुषमा रावत, मंडल अध्यक्ष बीजेपी जितेंद्र धिरवाण आदि मौजूद थे।